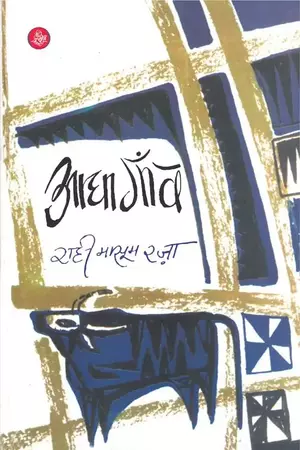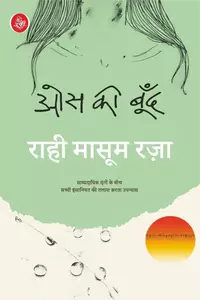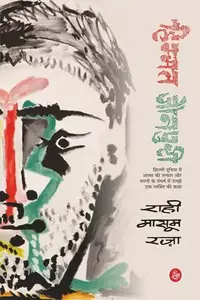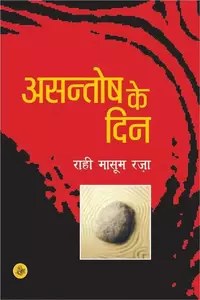|
उपन्यास >> आधा गाँव आधा गाँवराही मासूम रजा
|
389 पाठक हैं |
|||||||
"भारतीयता के रंगों में रचा-बसा उपन्यास, जो बँटवारे की त्रासदी में भी एकता की आवाज़ बुलंद करता है।"
प्रस्तुत है पुस्तक के कुछ अंश
ऊँघता शहर
ग़ाज़ीपुर के पुराने क़िले में अब एक स्कूल है जहाँ गंगा की लहरों की आवाज़ तो आती है, लेकिन इतिहास के गुनगुनाने या ठण्डी साँसे लेने की आवाज़ नहीं आती। क़िले की दीवारों पर अब कोई पहरेदार नहीं घूमता, न ही उन तक कोई विद्यार्थी ही आता है, जो डूबते हुए सूरज की रोशनी में चमचमाती हुई गंगा से कुछ कहे या सुने।
गँदले पानी की इस महान् धारा को न जाने कितनी कहानियाँ याद होंगी। परन्तु माँयें तो जिनों, परियों, भूतों और डाकुओं की कहानियों में मगन हैं और गंगा कि किनारे न जाने कब से मेल्हते हुए इस शहर को इसका खयाल भी नहीं आता कि गंगा के पाठशाले में बैठकर अपने पुरखों की कहानियाँ सुने।
यह असंभव नहीं कि अगर अब भी इस क़िले की पुरानी दीवार पर कोई आ बैठे और अपनी आँखें बन्द कर ले तो उस पार के गाँव और मैदान और खेत घने जंगलों में बदल जाएँ और तपोवन में ऋषियों की कुटियाँ दिखाई देने लगें। और वह देखे कि अयोध्या के दो राजकुमार कन्धे से कमानें लटकाये तपोवन के पवित्र सन्नाटे की रक्षा कर रहे हैं।
लेकिन इन दीवारों पर कोई बैठता ही नहीं। क्योंकि जब इन पर बैठने की उम्र आती है तो गज़भर की छातियों वाले बेरोजगारी के कोल्हू में जोत दिए जाते हैं कि वे अपने सपनों का तेल निकालें उस जहर को पीकर चुपचाप मर जायें।
गँदले पानी की इस महान् धारा को न जाने कितनी कहानियाँ याद होंगी। परन्तु माँयें तो जिनों, परियों, भूतों और डाकुओं की कहानियों में मगन हैं और गंगा कि किनारे न जाने कब से मेल्हते हुए इस शहर को इसका खयाल भी नहीं आता कि गंगा के पाठशाले में बैठकर अपने पुरखों की कहानियाँ सुने।
यह असंभव नहीं कि अगर अब भी इस क़िले की पुरानी दीवार पर कोई आ बैठे और अपनी आँखें बन्द कर ले तो उस पार के गाँव और मैदान और खेत घने जंगलों में बदल जाएँ और तपोवन में ऋषियों की कुटियाँ दिखाई देने लगें। और वह देखे कि अयोध्या के दो राजकुमार कन्धे से कमानें लटकाये तपोवन के पवित्र सन्नाटे की रक्षा कर रहे हैं।
लेकिन इन दीवारों पर कोई बैठता ही नहीं। क्योंकि जब इन पर बैठने की उम्र आती है तो गज़भर की छातियों वाले बेरोजगारी के कोल्हू में जोत दिए जाते हैं कि वे अपने सपनों का तेल निकालें उस जहर को पीकर चुपचाप मर जायें।
लगा झूलनी का धक्का
बलम कलकत्ता चले गये।
बलम कलकत्ता चले गये।
कलकत्ता की चटकलों में इस शहर के सपने सन के ताने-बाने में बुनकर दिसावर भेज दिये जाते हैं और फिर सिर्फ खाली आँखें रह जाती हैं और वीरान दिल रह जाते हैं और थके हुए बदन रह जाते हैं, जो किसी अँधेरी-सी कोठरी में पड़ रहते हैं जो पगडण्डियों, कच्चे-पक्के तालाबों, धान, जौ और मटर के खेतों को याद करते रहते हैं।
कलकत्ता !
कलकत्ता किसी शहर का नाम नहीं है। ग़ाज़ीपुर के बेटे-बेटियों के लिए यह भी विरह का एक नाम है। यह शब्द विरह की एक पूरी कहानी है, जिसमें न मालूम कितनी आँखों का काजल बहकर सूख चुका है। हर साल हज़ारों-हज़ार परदेस जानेवाले मेघदूत द्वारा हज़ारों-हज़ार सन्देश भेजते हैं। शायद इसीलिए ग़ाज़ीपुर में टूटकर पानी बरसता है और बरसात में नयी-पुरानी दीवारों, मस्जिदों और मंदिरों की छतों और स्कूलों की खिड़कियों के दरवाज़ों की दरार में विरह के अँखुये फूट आते हैं, और जुदाई का दर्द जाग उठता है और गाने लगते हैं :
कलकत्ता !
कलकत्ता किसी शहर का नाम नहीं है। ग़ाज़ीपुर के बेटे-बेटियों के लिए यह भी विरह का एक नाम है। यह शब्द विरह की एक पूरी कहानी है, जिसमें न मालूम कितनी आँखों का काजल बहकर सूख चुका है। हर साल हज़ारों-हज़ार परदेस जानेवाले मेघदूत द्वारा हज़ारों-हज़ार सन्देश भेजते हैं। शायद इसीलिए ग़ाज़ीपुर में टूटकर पानी बरसता है और बरसात में नयी-पुरानी दीवारों, मस्जिदों और मंदिरों की छतों और स्कूलों की खिड़कियों के दरवाज़ों की दरार में विरह के अँखुये फूट आते हैं, और जुदाई का दर्द जाग उठता है और गाने लगते हैं :
बरसत में कोऊ घर से न निकसे
तुमहिं अनूक विदेस जवैया।
तुमहिं अनूक विदेस जवैया।
कलकत्ता, बम्बई, कानपुर और ढाका—इस शहर की हदें हैं। दूर तक फैली हुई हदें....यहाँ के रहनेवाले यहाँ से जाकर भी यहीं के रहते हैं। गुब्बारे आकाश में चाहे कितनी दूर निकल जायँ परन्तु अपने केन्द्र से उनका सम्बन्ध नहीं टूटता, जहाँ किसी बच्चे के हाथ में निर्बल धागे का एक सिरा होता है।
इधर कुछ दिनों से ऐसा हो गया है कि बहुत से बच्चों के हाथों से यह डोर टूट गयी है।
यह कहानी सच पूछिये तो उन्हीं गुब्बारों की है या शायद उन बच्चों की जिनके हाथों में मरी हुई डोर का एक सिरा है और जो अपने ग़ुब्बारों को तलाश कर रहे हैं और जिन्हें यह नहीं मालूम कि डोर टूट जाने पर उन ग़ुब्बारों का अन्जाम क्या हुआ।
गंगा इस नगर के सिर पर और गालों पर हाथ फेरती रहती है; जैसे कोई माँ अपने बीमार बच्चे को प्यार कर रही हो, परन्तु जब इस प्यार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, तो गंगा बिलख-बिलखकर रोने लगती है और यह नगर उसके आँसुओं में डूब जाता है। लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गयी।
मुसलमान अज़ान देने लगते हैं। हिन्दू गंगा पर चढ़ावे चढ़ाने लगते हैं कि रूठी हुई गंगा मैया मान जाय। अपने प्यार की इस हनक पर गंगा झल्ला जाती है और क़िले की दीवार से अपनी सिर टकराने लगती है और उसमें उजले-सफेद बाल उलझकर दूर-दूर तक फैल जाते हैं। हम उसे झाग कहते हैं। गंगा जब यह देखती है कि उसके दुःख को कोई नहीं समझता, तो वह अपने आँसू पोंछ डालती है; तब हम यह कहते हैं कि पानी उतर गया। मुसलमान कहते हैं कि अज़ान का वार कभी खाली नहीं जाता, हिन्दू कहते हैं कि गंगा ने उनकी भेंट स्वीकार कर ली। और कोई यह नहीं कहता कि माँ के आँसुओं ने ज़मीन को भी उपजाऊ बना दिया है। दूर-दूर तक ज़मीन पर गर्म मिट्टी का एक ग़िलाफ़-सा चढ़ जाता है। परन्तु गंगा भी क्या करे, डाँगर-बैलों में हल का बोझ उठाने की ताक़त ही नहीं रही है।
यह शहर इतिहास से बेखबर है, इसे इतनी फ़ुरसत ही नहीं मिलती कि कभी बरगद की ठण्डी छाँव में लेटकर अपने इतिहास के विषय में सोचे; जो रामायण से आगे तक फैला हुआ है। रहा भविष्य, तो उसके विषय में सोचने का इसे साहस ही नहीं है। समय के घड़े में एक पतला सा छेद है जिससे क्षण-क्षण समय टपकता रहता है। यह शहर क्षण-क्षण जीता है क्षण-क्षण मरता है, और फिर जी उठता है।
कौन जाने इसकी यह घोर तपस्या कब खत्म हो। ग़ाज़ीपुर ज़िन्दगी के काफ़िलों के रास्ते पर नहीं है। कभी हवा इधर से होकर गुजरती है तो काफ़िलों की धूल आ जाती है और यह बस्ती उस धूल को इत्र की तरह अपने कपड़ों में अपने बदन पर मलकर खुश हो लेती है।
यह मेरा शहर है। मैं जब भी अपने शहर की गलियों से गुज़रता हूँ, यह मेरे कन्धे पर हाथ रख देता है। मेरी छोटी-छोटी कहानियों के रास्ते पर मुझे जगह-जगह मिलता है। परन्तु इसकी सम्पूर्ण वास्तविकता अब तक मेरे काबू में नहीं आयी है, इसलिए मैं इसे एक बार फिर देखना चाहता हूँ।
यह उपन्यास वास्तव में मेरा एक सफ़र है। मैं ग़ाज़ीपुर की तलाश में निकला हूँ, लेकिन पहले मैं अपने गंगौली में ठहरूँगा। अगर गंगौली की हक़ीक़त पकड़ में आ गयी तो मैं ग़ाज़ीपुर का ‘एपिक’ लिखने का साहस करूँगा। यह उपन्यास वास्तव में उस एपिक (महाकाव्य) की भूमिका है।
परन्तु एक बात सुन लीजिए। यह कहानी न कुछ लोगों की है और व कुछ परिवारों की। यह उस गाँव की कहानी भी नहीं है जिसमें इस कहानी के भले-बुरे पात्र अपने को पूर्ण बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह कहानी न धार्मिक है न राजनीतिक। क्योंकि समय न धार्मिक होता है, न राजनीतिक और यह कहानी है समय ही की। यह गंगौली में गुज़रने वाले समय की कहानी है।
कई बूढ़े मर गए, कई जवान बूढ़े हो गये, कई बच्चे जवान हो गये और कई बच्चे पैदा हो गये। यह उम्रों के इस हेर-फेर में फँसे हुए सपनों और हौसलों की कहानी है। यह कहानी है उन खंडहरों की जहाँ कभी मकान थे और यह कहानी है उन मकानों की जो कभी खण्डहरों पर बनाये गये हैं।
और यह कहानी जितनी सच्ची है उतनी ही झूठी भी।
मुझे झूठ में सच और सच में झूठ की मिलावट की कला आती है। इस कहानी में जगह-जगह ‘मैं’ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि यह कहानी मुझसे दूर न जा सके कि मैं जब चाहूँ इसे छू लूँ। अपने-आपको ढाँढ़स देने के लिए कि जो कहानी मैं सुना रहा हूँ वह आपको और अपने-आपको यह विश्वास दिलाने के लिए कि इसी कहानी की तरह मैं खुद भी हूँ। इसलिए यह आपबीती भी है और जगबीती भी।
युग एक बिना जिल्द की किताब की तरह एक खुले मैदान में पड़ा हुआ है। हवा की हल्की-सी लहर भी इसके पन्ने उलटती-पलटती रहती है। पढ़नेवाले के सामने पन्नों में फरसव घटते-बढ़ते रहते हैं, कभी वह दस पृष्ठ आगे निकल जाता है और कभी दस पृष्ठ पीछे रह जाता है। इसलिए मैं प्रथम पुरुष का बेखटके प्रयोग कर रहा हूँ कि पन्ने स्वयं न उलट सकें ताकि क्रम शेष रहे और मैं यह देख सकूँ कि क्या था, क्या है और क्या होनेवाला है।
कहते हैं कि आषाढ़ की काली रात में तुगलक के एक सरदार सय्यद मसउद ग़ाज़ी ने बाढ़ पर आयी गंगा को पार कर करके गादिपुरी पर हमला किया। चुनाँचे यह शहर गादिपुरी से ग़ाज़ीपुर हो गया। रास्ते वही हैं, गलियाँ भी वही रहीं, मकान भी वही रहे, नाम बदल गया—नाम शायद एक ऊपरी खोल होता है जिसे बदला जा सकता है। नाम का व्यक्तित्व से कोई अटूट रिश्ता नहीं होता शायद क्योंकि यदि ऐसा होता तो ग़ाज़ीपुर बनकर गादिपुरी को भी बदल जाना चाहिए या फिर कम-से-कम इतना होता कि हारनेवाले ठाकुर, ब्राह्मण, कायस्थ, अहीर, भर और चमार अपने को गादिपुरी कहते और जीतनेवाले सय्यद, शेख और पठान अपने को ग़ाज़ीपुरी। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। सब ग़ाज़ीपुरी हैं और अगर शहर का नाम न बदला होता तो सब गादिपुरी होते। ये नये नाम हैं बड़े दिलचस्प। अरबी का ‘फ़तह’ हिन्दी के ‘गढ़’ में घुलकर एक इकाई बन जाता है। इसीलिए तो पाकिस्तान बन जाने के बाद भी पाकिस्तान की हक़ीक़त मेरी समझ में नहीं आती। अगर ‘अली’ को ‘गढ़’ से, ‘गाजी’ को ‘पुर’ से और ‘दिलदार’ को ‘नगर’ से अलग कर दिया जाएगा तो बस्तियाँ वीरान और बेनाम हो जाएँगी और अगर ‘इमाम’ को बाड़े से निकाल दिया गया तो मोहर्रम कैसे होगा !
गंगा इस ग़ाज़ीपुर को भी उसी तरह सीने से लगाये हुए है जिस तरह वह गादिपुरी को लगाए हुए थी। इसलिए नाम गादिपुरी हो या ग़ाज़ीपुर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मसऊद ग़ाजी के बाल-बच्चों ने दूर-पास के देहातों पर जरूर कब्ज़ा जमाया होता। और यूँ दिल्ली से आने वाला खानदान कई ज़मींदार परिवारों में ज़रूर बढ़ता और मैं यह कहानी भी लिखता।
मसऊद ग़ाज़ी के एक लड़के, नूरुद्दीन शहीद ने (यह शहीद कैसे और क्यों हुए, यह मुझे नहीं मालूम और शायद किसी को नहीं मालूम) दो नदियाँ पार करके ग़ाज़ीपुर से कोई बारह-चौदह मील दूर, गंगौली को फ़तह किया। कहते हैं कि इस गाँव के राजा का नाम गंग था और उसी के नाम पर इस गाँव का नाम गंगौली पड़ा। लेकिन इस सय्यद ख़ानदान के पाँव जमने के बाद भी इस गाँव का नाम नूरपुर या नीरुद्दीन नगर नहीं हुआ—मेरी गंगौली का नाम मेरे ग़ाज़ीपुर से बुरा नहीं। लेकिन मज़े की बात यह है कि नूरुद्दीन शहीद की समाधि, जो गंगौली से नयी है, गंगौली से पुरानी मालूम होती है...ईंटों की इस छोटी-सी इमारत पर कभी एक छत जरूर रही होगी। परन्तु मैं तो लगभग छत्तीस-पैंतीस साल से इसे खण्डहर ही देख रहा हूँ। बस दस मोहर्रम को जब दोनों पट्टियों के जुलूस यहाँ आते हैं तो मजमा-सा लग जाता है और समाधि से जरा हटकर लड़की के अखाड़ेवाले अपना मजमा लगाकर गदके, बनैठी, बाँक और तलवार के हाथ निकालने लगते हैं और फिर एकदम से कोई आदमी नारा लगाता है-‘‘बोल मुहमुदी !’ और सारा गाँव जवाब देता है--‘या हुसैन का !!
इधर कुछ दिनों से गंगौलीवालों की संख्या कम होती जा रही है और सुन्नियों, शियों और हिन्दुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। शायद इसीलिए नूरुद्दीनकी की समाधि पर अब उतना बड़ा मजमा नहीं लगता और गंगौली का वातावरण ‘बोल मुहमुदी’ या हुसैन की आवाज़ से उस तरह नहीं गूँजता जिस तरह कभी गूँज उठा करता था। शायद यही कारण है कि समाधि आज उदास-उदास नजर आती है और अपनी अन्धी आँखों से इधर-उधर देखती रहती और सोचती रहती है—मेरी गंगौली कहाँ गयी ! लेकिन इस समाधि की जड़ें गंगौली की ज़मीन में है। इसीलिए वह जहाँ-की-तहाँ खड़ी है अकेली।
विशाल वृक्ष अपनी जगह से नहीं हटते, जब तक उन्हें काट न डाला जाय या जब तक कि उनकी जड़ें खोखली न हो जायँ। अबुल क़ासिम चा, बद्दन भाई, तन्नू भाई, तस्सन, क़ैसर, अख्तर और गिग्गे पाकिस्तान में है। परन्तु नूरुद्दीन शहीद की समाधि अब भी गंगौली में है और उसे कस्टोडियन ने भी नहीं हथियाया है क्योंकि कस्टोडियन को मालूम था कि यह नूरुद्दीन शहीद की समाधि गंगौली के सय्यदों की नहीं है बल्कि गंगौली की है। बरगद के पेड़ों की उम्र ज़रा लम्बी होती है और फिर इस समाधि को कई नस्लों ने अपनी-अपनी हड्डियों की खाद दी है।
इस समाधि के अतिरिक्त गंगौली के सय्यदों ने एक ‘कर्बला’ भी बनवाया। यह कर्बला समाधि के दक्षिण में है और खुद समाधि गंगौली के पूरब में है। इन लोगों ने एक तालाब भी खुदवाया जो गाँव के पश्चिमी सिरे पर है। यह तालाब नूरुद्दीन शहीद के उत्तराधिकारियों ने ही बनवाया होगा, क्योंकि इसके आसपास किसी मन्दिर का निशान नहीं है। तालाब से निकली हुई मिट्टी के टीलों पर आम और जामुन के पेड़ हैं और गाँव के मीर साहिबान दस मोहर्रम को, इन्हीं टीलों पर नमाज़ पढ़ने आते हैं। इस तालाब के पश्चिम में चूने का बना हुआ तीन दरों वाला नील का एक वीरान कारख़ाना है जिसे हम लोग न मालूम क्यों गोदाम कहते हैं। यह जॉन गिलक्राइस्ट की यादगार है यानी एक और ही युग की निशानी है। अब तो यह सिर्फ़ चरवाहों के काम आता है जो उस बैठकर ईख खाते हैं और यह प्रेमियों के काम आता है। यहाँ चाहे हीर को राँझा न मिलता हो, परन्तु बदन को बदन अवश्य मिल जाता है।
एक टूटी-फूटी समाधि और एक उजड़े हुए कारख़ाने के बीच में यह गाँव आबाद है। गंगौली के कोनों पर सय्यद लोगों के मकान हैं। कुल मिलाकर दस घर होंगे। दक्षिणवाले घर दक्षिणी पट्टी कहलाते हैं और उत्तरवाले उत्तरी पट्टी। बीच में जुलाहों के घर हैं। सिब्तू दा के घर से राक़ियों की आबादी शुरू हो जाती है और फिर गन्दी, कच्ची गली गंगौली के बाज़ार में दाख़िल हो जाती है और नीची दुकानों और खुजली के मारे हुए कुत्तों से दबकर गुज़रती हुई नूरुद्दीन शहीद की समाधि के खुले हुए वातावरण में आकर इत्मीनान की साँसें लेती है।
गाँव के आस-पास झोपड़ों के कई ‘पूरे’ आबाद हैं। किसी में चमार रहते हैं, किसी में भर और किसी में अहीर। गंगौली में तीन बड़े दरवाज़े हैं। एक उत्तर पट्टी में और पक्कड़ तले कहा जाता है। यह लकड़ी का एक बड़ा-सा फाटक है। सामने ही पक्कड़ का एक पेड़ है। चौखट से उतरते ही दाहिनी तरफ कई इमाम चौक हैं जिन पर नौ मोहर्रम की लकड़ी के खूबसूरत ताज़िए रखे जाते हैं और फिर एक बड़ा आँगन है। ज़मींदारों में इन बड़े आँगनो का एक बड़ा सामाजिक महत्त्व है। आसामियों की बरातें यहीं उतरती है, मरने-जीने का खाना यहीं होता है। आसामियों को सज़ा यहीं दी जाती है। पट्टीदारी के मामले यहीं उलझाए जाते हैं और सुलझाये जाते हैं और यहीं थानेदारों, डिप्टियों और कलक्टरों का नाच-रंग होता है—ये आँगन न हों तो ज़मीदारियाँ ही न चले। तो एक बड़ा फाटक उत्तर पट्टी में भी है और दो दक्षिण पट्टी में। एक जहीर चा के पुरखों का, यानी दद्दा के मायकेवालों का। इस फाटक का नाम ‘बड़का’ फाटक है। और बड़ा दरवाज़ा अब्बू दा के बुज़ुर्गों का है जो ! अब्बू मियाँ का फाटक’ कहा जाता है।
हमें इन्हीं तीनों और इनके चारों तरफ रहनेवाले सय्यद परिवारों में जाना है।
हाँ, एक बात और। यह गंगौली कोई काल्पनिक गाँव नहीं है और इस गाँव में जो घर नज़र आएँगे वे भी काल्पनिक नहीं है। मैंने तो केवल इतना किया है इन मकानों मकानवालों से ख़ाली करवाकर इस उपन्यास के पात्रों को बसा दिया है। ये पात्र ऐसे हैं कि इस वातावरण में अजनबी नहीं मालूम, होंगे और शायद आप भी अनुभव करें कि फुन्नन मियाँ, अब्बू मियाँ, झंगटिया बो, मौलवी बेदार, कोमिला, बबरमुआ, बलराम चमार, हकीम अली कबीर, गया अहीर और अनवारुलहसन’ राक़ी और दूसरे तमाम लोग भी गंगौली के रहने वाले हैं लेकिन मैंने इन काल्पनिक पात्रों में कुछ असल पात्रों को भी फेंट दिया है। ये असली पात्र मेरा घरवाले हैं जिनसे मैंने यथार्थ की पृष्ठभूमि बनायी है और जिनके कारण इस कहानी के काल्पनिक पात्र भी मुझसे बेतकल्लुफ़ हो गये हैं।
आइए, अब चलें।
इधर कुछ दिनों से ऐसा हो गया है कि बहुत से बच्चों के हाथों से यह डोर टूट गयी है।
यह कहानी सच पूछिये तो उन्हीं गुब्बारों की है या शायद उन बच्चों की जिनके हाथों में मरी हुई डोर का एक सिरा है और जो अपने ग़ुब्बारों को तलाश कर रहे हैं और जिन्हें यह नहीं मालूम कि डोर टूट जाने पर उन ग़ुब्बारों का अन्जाम क्या हुआ।
गंगा इस नगर के सिर पर और गालों पर हाथ फेरती रहती है; जैसे कोई माँ अपने बीमार बच्चे को प्यार कर रही हो, परन्तु जब इस प्यार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, तो गंगा बिलख-बिलखकर रोने लगती है और यह नगर उसके आँसुओं में डूब जाता है। लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गयी।
मुसलमान अज़ान देने लगते हैं। हिन्दू गंगा पर चढ़ावे चढ़ाने लगते हैं कि रूठी हुई गंगा मैया मान जाय। अपने प्यार की इस हनक पर गंगा झल्ला जाती है और क़िले की दीवार से अपनी सिर टकराने लगती है और उसमें उजले-सफेद बाल उलझकर दूर-दूर तक फैल जाते हैं। हम उसे झाग कहते हैं। गंगा जब यह देखती है कि उसके दुःख को कोई नहीं समझता, तो वह अपने आँसू पोंछ डालती है; तब हम यह कहते हैं कि पानी उतर गया। मुसलमान कहते हैं कि अज़ान का वार कभी खाली नहीं जाता, हिन्दू कहते हैं कि गंगा ने उनकी भेंट स्वीकार कर ली। और कोई यह नहीं कहता कि माँ के आँसुओं ने ज़मीन को भी उपजाऊ बना दिया है। दूर-दूर तक ज़मीन पर गर्म मिट्टी का एक ग़िलाफ़-सा चढ़ जाता है। परन्तु गंगा भी क्या करे, डाँगर-बैलों में हल का बोझ उठाने की ताक़त ही नहीं रही है।
यह शहर इतिहास से बेखबर है, इसे इतनी फ़ुरसत ही नहीं मिलती कि कभी बरगद की ठण्डी छाँव में लेटकर अपने इतिहास के विषय में सोचे; जो रामायण से आगे तक फैला हुआ है। रहा भविष्य, तो उसके विषय में सोचने का इसे साहस ही नहीं है। समय के घड़े में एक पतला सा छेद है जिससे क्षण-क्षण समय टपकता रहता है। यह शहर क्षण-क्षण जीता है क्षण-क्षण मरता है, और फिर जी उठता है।
कौन जाने इसकी यह घोर तपस्या कब खत्म हो। ग़ाज़ीपुर ज़िन्दगी के काफ़िलों के रास्ते पर नहीं है। कभी हवा इधर से होकर गुजरती है तो काफ़िलों की धूल आ जाती है और यह बस्ती उस धूल को इत्र की तरह अपने कपड़ों में अपने बदन पर मलकर खुश हो लेती है।
यह मेरा शहर है। मैं जब भी अपने शहर की गलियों से गुज़रता हूँ, यह मेरे कन्धे पर हाथ रख देता है। मेरी छोटी-छोटी कहानियों के रास्ते पर मुझे जगह-जगह मिलता है। परन्तु इसकी सम्पूर्ण वास्तविकता अब तक मेरे काबू में नहीं आयी है, इसलिए मैं इसे एक बार फिर देखना चाहता हूँ।
यह उपन्यास वास्तव में मेरा एक सफ़र है। मैं ग़ाज़ीपुर की तलाश में निकला हूँ, लेकिन पहले मैं अपने गंगौली में ठहरूँगा। अगर गंगौली की हक़ीक़त पकड़ में आ गयी तो मैं ग़ाज़ीपुर का ‘एपिक’ लिखने का साहस करूँगा। यह उपन्यास वास्तव में उस एपिक (महाकाव्य) की भूमिका है।
परन्तु एक बात सुन लीजिए। यह कहानी न कुछ लोगों की है और व कुछ परिवारों की। यह उस गाँव की कहानी भी नहीं है जिसमें इस कहानी के भले-बुरे पात्र अपने को पूर्ण बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह कहानी न धार्मिक है न राजनीतिक। क्योंकि समय न धार्मिक होता है, न राजनीतिक और यह कहानी है समय ही की। यह गंगौली में गुज़रने वाले समय की कहानी है।
कई बूढ़े मर गए, कई जवान बूढ़े हो गये, कई बच्चे जवान हो गये और कई बच्चे पैदा हो गये। यह उम्रों के इस हेर-फेर में फँसे हुए सपनों और हौसलों की कहानी है। यह कहानी है उन खंडहरों की जहाँ कभी मकान थे और यह कहानी है उन मकानों की जो कभी खण्डहरों पर बनाये गये हैं।
और यह कहानी जितनी सच्ची है उतनी ही झूठी भी।
मुझे झूठ में सच और सच में झूठ की मिलावट की कला आती है। इस कहानी में जगह-जगह ‘मैं’ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि यह कहानी मुझसे दूर न जा सके कि मैं जब चाहूँ इसे छू लूँ। अपने-आपको ढाँढ़स देने के लिए कि जो कहानी मैं सुना रहा हूँ वह आपको और अपने-आपको यह विश्वास दिलाने के लिए कि इसी कहानी की तरह मैं खुद भी हूँ। इसलिए यह आपबीती भी है और जगबीती भी।
युग एक बिना जिल्द की किताब की तरह एक खुले मैदान में पड़ा हुआ है। हवा की हल्की-सी लहर भी इसके पन्ने उलटती-पलटती रहती है। पढ़नेवाले के सामने पन्नों में फरसव घटते-बढ़ते रहते हैं, कभी वह दस पृष्ठ आगे निकल जाता है और कभी दस पृष्ठ पीछे रह जाता है। इसलिए मैं प्रथम पुरुष का बेखटके प्रयोग कर रहा हूँ कि पन्ने स्वयं न उलट सकें ताकि क्रम शेष रहे और मैं यह देख सकूँ कि क्या था, क्या है और क्या होनेवाला है।
कहते हैं कि आषाढ़ की काली रात में तुगलक के एक सरदार सय्यद मसउद ग़ाज़ी ने बाढ़ पर आयी गंगा को पार कर करके गादिपुरी पर हमला किया। चुनाँचे यह शहर गादिपुरी से ग़ाज़ीपुर हो गया। रास्ते वही हैं, गलियाँ भी वही रहीं, मकान भी वही रहे, नाम बदल गया—नाम शायद एक ऊपरी खोल होता है जिसे बदला जा सकता है। नाम का व्यक्तित्व से कोई अटूट रिश्ता नहीं होता शायद क्योंकि यदि ऐसा होता तो ग़ाज़ीपुर बनकर गादिपुरी को भी बदल जाना चाहिए या फिर कम-से-कम इतना होता कि हारनेवाले ठाकुर, ब्राह्मण, कायस्थ, अहीर, भर और चमार अपने को गादिपुरी कहते और जीतनेवाले सय्यद, शेख और पठान अपने को ग़ाज़ीपुरी। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। सब ग़ाज़ीपुरी हैं और अगर शहर का नाम न बदला होता तो सब गादिपुरी होते। ये नये नाम हैं बड़े दिलचस्प। अरबी का ‘फ़तह’ हिन्दी के ‘गढ़’ में घुलकर एक इकाई बन जाता है। इसीलिए तो पाकिस्तान बन जाने के बाद भी पाकिस्तान की हक़ीक़त मेरी समझ में नहीं आती। अगर ‘अली’ को ‘गढ़’ से, ‘गाजी’ को ‘पुर’ से और ‘दिलदार’ को ‘नगर’ से अलग कर दिया जाएगा तो बस्तियाँ वीरान और बेनाम हो जाएँगी और अगर ‘इमाम’ को बाड़े से निकाल दिया गया तो मोहर्रम कैसे होगा !
गंगा इस ग़ाज़ीपुर को भी उसी तरह सीने से लगाये हुए है जिस तरह वह गादिपुरी को लगाए हुए थी। इसलिए नाम गादिपुरी हो या ग़ाज़ीपुर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मसऊद ग़ाजी के बाल-बच्चों ने दूर-पास के देहातों पर जरूर कब्ज़ा जमाया होता। और यूँ दिल्ली से आने वाला खानदान कई ज़मींदार परिवारों में ज़रूर बढ़ता और मैं यह कहानी भी लिखता।
मसऊद ग़ाज़ी के एक लड़के, नूरुद्दीन शहीद ने (यह शहीद कैसे और क्यों हुए, यह मुझे नहीं मालूम और शायद किसी को नहीं मालूम) दो नदियाँ पार करके ग़ाज़ीपुर से कोई बारह-चौदह मील दूर, गंगौली को फ़तह किया। कहते हैं कि इस गाँव के राजा का नाम गंग था और उसी के नाम पर इस गाँव का नाम गंगौली पड़ा। लेकिन इस सय्यद ख़ानदान के पाँव जमने के बाद भी इस गाँव का नाम नूरपुर या नीरुद्दीन नगर नहीं हुआ—मेरी गंगौली का नाम मेरे ग़ाज़ीपुर से बुरा नहीं। लेकिन मज़े की बात यह है कि नूरुद्दीन शहीद की समाधि, जो गंगौली से नयी है, गंगौली से पुरानी मालूम होती है...ईंटों की इस छोटी-सी इमारत पर कभी एक छत जरूर रही होगी। परन्तु मैं तो लगभग छत्तीस-पैंतीस साल से इसे खण्डहर ही देख रहा हूँ। बस दस मोहर्रम को जब दोनों पट्टियों के जुलूस यहाँ आते हैं तो मजमा-सा लग जाता है और समाधि से जरा हटकर लड़की के अखाड़ेवाले अपना मजमा लगाकर गदके, बनैठी, बाँक और तलवार के हाथ निकालने लगते हैं और फिर एकदम से कोई आदमी नारा लगाता है-‘‘बोल मुहमुदी !’ और सारा गाँव जवाब देता है--‘या हुसैन का !!
इधर कुछ दिनों से गंगौलीवालों की संख्या कम होती जा रही है और सुन्नियों, शियों और हिन्दुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। शायद इसीलिए नूरुद्दीनकी की समाधि पर अब उतना बड़ा मजमा नहीं लगता और गंगौली का वातावरण ‘बोल मुहमुदी’ या हुसैन की आवाज़ से उस तरह नहीं गूँजता जिस तरह कभी गूँज उठा करता था। शायद यही कारण है कि समाधि आज उदास-उदास नजर आती है और अपनी अन्धी आँखों से इधर-उधर देखती रहती और सोचती रहती है—मेरी गंगौली कहाँ गयी ! लेकिन इस समाधि की जड़ें गंगौली की ज़मीन में है। इसीलिए वह जहाँ-की-तहाँ खड़ी है अकेली।
विशाल वृक्ष अपनी जगह से नहीं हटते, जब तक उन्हें काट न डाला जाय या जब तक कि उनकी जड़ें खोखली न हो जायँ। अबुल क़ासिम चा, बद्दन भाई, तन्नू भाई, तस्सन, क़ैसर, अख्तर और गिग्गे पाकिस्तान में है। परन्तु नूरुद्दीन शहीद की समाधि अब भी गंगौली में है और उसे कस्टोडियन ने भी नहीं हथियाया है क्योंकि कस्टोडियन को मालूम था कि यह नूरुद्दीन शहीद की समाधि गंगौली के सय्यदों की नहीं है बल्कि गंगौली की है। बरगद के पेड़ों की उम्र ज़रा लम्बी होती है और फिर इस समाधि को कई नस्लों ने अपनी-अपनी हड्डियों की खाद दी है।
इस समाधि के अतिरिक्त गंगौली के सय्यदों ने एक ‘कर्बला’ भी बनवाया। यह कर्बला समाधि के दक्षिण में है और खुद समाधि गंगौली के पूरब में है। इन लोगों ने एक तालाब भी खुदवाया जो गाँव के पश्चिमी सिरे पर है। यह तालाब नूरुद्दीन शहीद के उत्तराधिकारियों ने ही बनवाया होगा, क्योंकि इसके आसपास किसी मन्दिर का निशान नहीं है। तालाब से निकली हुई मिट्टी के टीलों पर आम और जामुन के पेड़ हैं और गाँव के मीर साहिबान दस मोहर्रम को, इन्हीं टीलों पर नमाज़ पढ़ने आते हैं। इस तालाब के पश्चिम में चूने का बना हुआ तीन दरों वाला नील का एक वीरान कारख़ाना है जिसे हम लोग न मालूम क्यों गोदाम कहते हैं। यह जॉन गिलक्राइस्ट की यादगार है यानी एक और ही युग की निशानी है। अब तो यह सिर्फ़ चरवाहों के काम आता है जो उस बैठकर ईख खाते हैं और यह प्रेमियों के काम आता है। यहाँ चाहे हीर को राँझा न मिलता हो, परन्तु बदन को बदन अवश्य मिल जाता है।
एक टूटी-फूटी समाधि और एक उजड़े हुए कारख़ाने के बीच में यह गाँव आबाद है। गंगौली के कोनों पर सय्यद लोगों के मकान हैं। कुल मिलाकर दस घर होंगे। दक्षिणवाले घर दक्षिणी पट्टी कहलाते हैं और उत्तरवाले उत्तरी पट्टी। बीच में जुलाहों के घर हैं। सिब्तू दा के घर से राक़ियों की आबादी शुरू हो जाती है और फिर गन्दी, कच्ची गली गंगौली के बाज़ार में दाख़िल हो जाती है और नीची दुकानों और खुजली के मारे हुए कुत्तों से दबकर गुज़रती हुई नूरुद्दीन शहीद की समाधि के खुले हुए वातावरण में आकर इत्मीनान की साँसें लेती है।
गाँव के आस-पास झोपड़ों के कई ‘पूरे’ आबाद हैं। किसी में चमार रहते हैं, किसी में भर और किसी में अहीर। गंगौली में तीन बड़े दरवाज़े हैं। एक उत्तर पट्टी में और पक्कड़ तले कहा जाता है। यह लकड़ी का एक बड़ा-सा फाटक है। सामने ही पक्कड़ का एक पेड़ है। चौखट से उतरते ही दाहिनी तरफ कई इमाम चौक हैं जिन पर नौ मोहर्रम की लकड़ी के खूबसूरत ताज़िए रखे जाते हैं और फिर एक बड़ा आँगन है। ज़मींदारों में इन बड़े आँगनो का एक बड़ा सामाजिक महत्त्व है। आसामियों की बरातें यहीं उतरती है, मरने-जीने का खाना यहीं होता है। आसामियों को सज़ा यहीं दी जाती है। पट्टीदारी के मामले यहीं उलझाए जाते हैं और सुलझाये जाते हैं और यहीं थानेदारों, डिप्टियों और कलक्टरों का नाच-रंग होता है—ये आँगन न हों तो ज़मीदारियाँ ही न चले। तो एक बड़ा फाटक उत्तर पट्टी में भी है और दो दक्षिण पट्टी में। एक जहीर चा के पुरखों का, यानी दद्दा के मायकेवालों का। इस फाटक का नाम ‘बड़का’ फाटक है। और बड़ा दरवाज़ा अब्बू दा के बुज़ुर्गों का है जो ! अब्बू मियाँ का फाटक’ कहा जाता है।
हमें इन्हीं तीनों और इनके चारों तरफ रहनेवाले सय्यद परिवारों में जाना है।
हाँ, एक बात और। यह गंगौली कोई काल्पनिक गाँव नहीं है और इस गाँव में जो घर नज़र आएँगे वे भी काल्पनिक नहीं है। मैंने तो केवल इतना किया है इन मकानों मकानवालों से ख़ाली करवाकर इस उपन्यास के पात्रों को बसा दिया है। ये पात्र ऐसे हैं कि इस वातावरण में अजनबी नहीं मालूम, होंगे और शायद आप भी अनुभव करें कि फुन्नन मियाँ, अब्बू मियाँ, झंगटिया बो, मौलवी बेदार, कोमिला, बबरमुआ, बलराम चमार, हकीम अली कबीर, गया अहीर और अनवारुलहसन’ राक़ी और दूसरे तमाम लोग भी गंगौली के रहने वाले हैं लेकिन मैंने इन काल्पनिक पात्रों में कुछ असल पात्रों को भी फेंट दिया है। ये असली पात्र मेरा घरवाले हैं जिनसे मैंने यथार्थ की पृष्ठभूमि बनायी है और जिनके कारण इस कहानी के काल्पनिक पात्र भी मुझसे बेतकल्लुफ़ हो गये हैं।
आइए, अब चलें।
मेरा गाँव, मेरे लोग
मैं गोरी दादी के आँगन से भागता हुआ दक्खिन वाले तीन-दर्रे में घुस गया। ठोकर लगी, गिर पड़ा। भाई साहब मेरे पीछे-पीछे भागे आ रहे थे। बात यह हुई थी कि बाजी ने धनया बनाकर बक्स में छुपा रखी थी। हमने देख लिया। धनया ख़त्म हो गयी। बाजी ने अम्माँ से शिकायत की। अम्माँ ने हमें दौड़ा लिया— इसलिए हम भाग रहे थे।
भाई साहब ने लपककर मुझे उठाया ही था कि अम्माँ का हाथ सिर पर दिखायी दिया। मैं तो गिरई मछली की तड़पकर उनके हाथों से निकल गया। लेकिन भाई साहब के बाल अम्माँ के हाथों में आ गये। मैं चुपचाप वहाँ से सरक लिया। सामने ही नईमा दादी की ख़लवत का छोटा-सा दरवाज़ा था, मैं ख़लवत में घुस गया।
ख़लवत के छोटे-से आँगन में अमरूद के एक पेड़ के बाद कुछ बचता ही नहीं था, मुश्किल से दो खटोले पड़ जाते थे, उनमें से एक खटोले पर नइमा दादी लेटी हुई तसबीह फेर रही थी; और उनके सिर के पास से गुज़रनेवाली अलगनी पर दो काले कुरते, दो काले आड़े पाजामे और दो काले दुपट्टे पड़े हुए सूख रहे थे। एक दुपट्टे के कोने से काला रंग बूँद-बूँद टपक रहा था और खटोले की सुतली को भिगो रहा था।
मुझे नहीं मालूम कि मँझले दादा के अब्बा को इन नइमा दादी में ऐसी कौन-सी बात नज़र आयी थी कि उन्होंने एक अच्छी-खासी गोरी-चिट्टी दादी को छोड़कर करइल मिट्टी की इस पुतली को निक़ाह में ले लिया और फिर उनके लिए उन्होंने यह ख़लवत बनवायी। नईमा दादी बहरहाल जुलाहिन थीं और सैदानियों के साथ नहीं रह सकती थीं। पुराने ज़माने के लोग इसका बड़ा ख़याल रखा करते थे कि कौन कहाँ बैठ सकता है और कहाँ नहीं। मेरी समझ में ये बातें नहीं आतीं, लेकिन मेरी समझ में तो और बहुत-सी बातें भी नहीं आतीं। मेरे समझ में तो यह भी नहीं आता कि मँझले दा के एकलौते बेटे गुज्जन मियाँ उर्फ़ सैयद ग़ज़नफ़र हुसैन ज़ैदी यानी छोटे दा ने एक अच्छी-ख़ासी, गोरी-चिट्टी, गोल-मटोल, चिकनी-चुपड़ी हुस्सन दादी को छोड़कर ज़मुर्रुद नामी एक रण्डी को क्यों रख लिया ? मैंने ज़मुर्रुद को नहीं देखा है, लेकिन हुस्सन दादी को मैंने अपनी आँख खोलने से लेकर उसकी आँख बन्द हो जाने तक देखा है। वह बड़ी कंजूस थीं, मगर बड़ी ख़ूबसूरत थीं। ज़मुर्रुद को गंगौली की किसी औरत ने नहीं देखा था, मगर सभी का यह ख़याल था कि उसने गुज्जन मियाँ पर कोई टोना-टोटका कर दिया है; इसीलिए गंगौली की तमाम औरतों को पक्का यक़ीन था कि वह बंगालिन है, हालाँकि वह बाराबंकी की थी।
लेकिन गंगौली की औरतों को गुज्जन मियाँ से यह शिकायत नहीं थी कि उन्होंने कोई रण्डी डाल ली है। रण्डी डाल लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन हुस्सन जैसी खूबसूरत बीवी को छोड़ना अलबत्ता गुनाह है। आख़िर अतहर मियाँ ने कानी दुल्हन यानी राबेया बीवी से निभायी कि नहीं ! जबकि अतहर मियाँ की गिनती खूबसूरतों में होती थी। मगर उन्हें खुदा करवट-करवट जन्नत दे, उन्होंने कभी कानी दुल्हन का दिल न मैला होने दिया, जबकि उन्हीं दिनों उस खाहुनपीटी जिनती नाइन की जवानी ऐसी फटी पड़ रही थी कि मियाँ लोग पोगल हुए जा रहे थे, और हर ब्याहता को इसका धड़का लगा रहता कि कब उसके आँगन में एक ख़लवत बन जाएगी। लेकिन अतहर मियाँ ने उसकी तरफ न देखा कि दुल्हन का दिल मैला होगा—और वह मुई जितनी चुई जा रही थी उन पर....
मगर जिस तरह मेरी समझ में नईमा दादी और ज़मुर्रूद का कहानी नहीं आती, उसी तरह मेरी समझ में यह भी नहीं आता की जब रब्बन बी कानी थी, और अतहर मियाँ बिलकुल चन्दे आफ़ताब और चन्दे माहताब थे, और जिनती नाइन उन पर चुभी जा रही थी, तो आख़िर उन्होंने अपना दामन क्यों नहीं फैलाया ?
दूसरा ब्याह कर लेना या किसी ऐरी-ग़ैरी औरत को घर में डाल लेना बुरा नहीं समझा जाता था, शायद ही मियाँ लोगों का कोई ऐसा खानदान हो, जिसमें क़लमी लड़के और लड़कियाँ न हों। जिनके घर में खाने को भी नहीं होता वे भी किसी-न-किसी तरह क़लमी आमों और क़लमी परिवार का शौक़ पूरा कर ही लेते हैं !
बस एक मीर अतहर हुसैन ज़ैदी ने ऐसा नहीं किया। वह पूरा साल अफ़ीम खा-खाकर मोहर्रम की तैयारियों में सर्फ़ दिया करते थे। उन्होंने अपनी जारी जिन्दगी ही मोहर्रम की तैयारियों में गुज़ार दी।
सच तो यह है कि उन दिनों सारा साल मोहर्रम के इन्तज़ार ही में कट जाता था। ईद की ख़ुशी अपनी जगह, मगर मोहर्रम की खुशी भी कुछ कम नहीं हुआ करती थी। बक़रीद के बाद से ही मोहर्रम की तैयारी शुरू हो जाती। दद्दा मरसिये गुनगुनाना शुरू कर देने, अम्माँ हम सब के लिए काले कपड़े सीने में लग जातीं; और बाजी नौहों की बयाज़े निकालकर नयी-नयी धुनों की मश्क़ करने लगतीं। उन दिनों नौहे की धुनों पर फ़िल्मी म्यूज़िक का क़ब्ज़ा नहीं हुआ था। नौहों की धुनें देहातों, क़स्बों और छोटे-मोटे शहरों की लोक-धुनों की तरह सादा और साथ-ही-साथ गम्भीर हुआ करती थीं, और जब बाजी, अम्माँ या कोई और खाला या फूफी काले कपड़े पहनकर नौहा पढ़ने खडी़ होतीं :
सोते-सोते सकीना यह कहती उठी शह का सीना नहीं तो सकीना नहीं...तो बयाज़ सँभालनेवाली कलाइयाँ एकदम से बदल जातीं। सुननेवालों को ऐसा मालूम होता जैसे नौहे की आवाज़ खास दमिश्क के बन्दीघर से आ रही है, और देखनेवाली आँखें देख लेतीं कि एक ज़मीनदोज़ क़ैदख़ाने में हुसैन की बहन ज़ैनब हुसैन की चहेती बेटी सकीना को बहलाने की कोशिश कर रही है...
भाई साहब ने लपककर मुझे उठाया ही था कि अम्माँ का हाथ सिर पर दिखायी दिया। मैं तो गिरई मछली की तड़पकर उनके हाथों से निकल गया। लेकिन भाई साहब के बाल अम्माँ के हाथों में आ गये। मैं चुपचाप वहाँ से सरक लिया। सामने ही नईमा दादी की ख़लवत का छोटा-सा दरवाज़ा था, मैं ख़लवत में घुस गया।
ख़लवत के छोटे-से आँगन में अमरूद के एक पेड़ के बाद कुछ बचता ही नहीं था, मुश्किल से दो खटोले पड़ जाते थे, उनमें से एक खटोले पर नइमा दादी लेटी हुई तसबीह फेर रही थी; और उनके सिर के पास से गुज़रनेवाली अलगनी पर दो काले कुरते, दो काले आड़े पाजामे और दो काले दुपट्टे पड़े हुए सूख रहे थे। एक दुपट्टे के कोने से काला रंग बूँद-बूँद टपक रहा था और खटोले की सुतली को भिगो रहा था।
मुझे नहीं मालूम कि मँझले दादा के अब्बा को इन नइमा दादी में ऐसी कौन-सी बात नज़र आयी थी कि उन्होंने एक अच्छी-खासी गोरी-चिट्टी दादी को छोड़कर करइल मिट्टी की इस पुतली को निक़ाह में ले लिया और फिर उनके लिए उन्होंने यह ख़लवत बनवायी। नईमा दादी बहरहाल जुलाहिन थीं और सैदानियों के साथ नहीं रह सकती थीं। पुराने ज़माने के लोग इसका बड़ा ख़याल रखा करते थे कि कौन कहाँ बैठ सकता है और कहाँ नहीं। मेरी समझ में ये बातें नहीं आतीं, लेकिन मेरी समझ में तो और बहुत-सी बातें भी नहीं आतीं। मेरे समझ में तो यह भी नहीं आता कि मँझले दा के एकलौते बेटे गुज्जन मियाँ उर्फ़ सैयद ग़ज़नफ़र हुसैन ज़ैदी यानी छोटे दा ने एक अच्छी-ख़ासी, गोरी-चिट्टी, गोल-मटोल, चिकनी-चुपड़ी हुस्सन दादी को छोड़कर ज़मुर्रुद नामी एक रण्डी को क्यों रख लिया ? मैंने ज़मुर्रुद को नहीं देखा है, लेकिन हुस्सन दादी को मैंने अपनी आँख खोलने से लेकर उसकी आँख बन्द हो जाने तक देखा है। वह बड़ी कंजूस थीं, मगर बड़ी ख़ूबसूरत थीं। ज़मुर्रुद को गंगौली की किसी औरत ने नहीं देखा था, मगर सभी का यह ख़याल था कि उसने गुज्जन मियाँ पर कोई टोना-टोटका कर दिया है; इसीलिए गंगौली की तमाम औरतों को पक्का यक़ीन था कि वह बंगालिन है, हालाँकि वह बाराबंकी की थी।
लेकिन गंगौली की औरतों को गुज्जन मियाँ से यह शिकायत नहीं थी कि उन्होंने कोई रण्डी डाल ली है। रण्डी डाल लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन हुस्सन जैसी खूबसूरत बीवी को छोड़ना अलबत्ता गुनाह है। आख़िर अतहर मियाँ ने कानी दुल्हन यानी राबेया बीवी से निभायी कि नहीं ! जबकि अतहर मियाँ की गिनती खूबसूरतों में होती थी। मगर उन्हें खुदा करवट-करवट जन्नत दे, उन्होंने कभी कानी दुल्हन का दिल न मैला होने दिया, जबकि उन्हीं दिनों उस खाहुनपीटी जिनती नाइन की जवानी ऐसी फटी पड़ रही थी कि मियाँ लोग पोगल हुए जा रहे थे, और हर ब्याहता को इसका धड़का लगा रहता कि कब उसके आँगन में एक ख़लवत बन जाएगी। लेकिन अतहर मियाँ ने उसकी तरफ न देखा कि दुल्हन का दिल मैला होगा—और वह मुई जितनी चुई जा रही थी उन पर....
मगर जिस तरह मेरी समझ में नईमा दादी और ज़मुर्रूद का कहानी नहीं आती, उसी तरह मेरी समझ में यह भी नहीं आता की जब रब्बन बी कानी थी, और अतहर मियाँ बिलकुल चन्दे आफ़ताब और चन्दे माहताब थे, और जिनती नाइन उन पर चुभी जा रही थी, तो आख़िर उन्होंने अपना दामन क्यों नहीं फैलाया ?
दूसरा ब्याह कर लेना या किसी ऐरी-ग़ैरी औरत को घर में डाल लेना बुरा नहीं समझा जाता था, शायद ही मियाँ लोगों का कोई ऐसा खानदान हो, जिसमें क़लमी लड़के और लड़कियाँ न हों। जिनके घर में खाने को भी नहीं होता वे भी किसी-न-किसी तरह क़लमी आमों और क़लमी परिवार का शौक़ पूरा कर ही लेते हैं !
बस एक मीर अतहर हुसैन ज़ैदी ने ऐसा नहीं किया। वह पूरा साल अफ़ीम खा-खाकर मोहर्रम की तैयारियों में सर्फ़ दिया करते थे। उन्होंने अपनी जारी जिन्दगी ही मोहर्रम की तैयारियों में गुज़ार दी।
सच तो यह है कि उन दिनों सारा साल मोहर्रम के इन्तज़ार ही में कट जाता था। ईद की ख़ुशी अपनी जगह, मगर मोहर्रम की खुशी भी कुछ कम नहीं हुआ करती थी। बक़रीद के बाद से ही मोहर्रम की तैयारी शुरू हो जाती। दद्दा मरसिये गुनगुनाना शुरू कर देने, अम्माँ हम सब के लिए काले कपड़े सीने में लग जातीं; और बाजी नौहों की बयाज़े निकालकर नयी-नयी धुनों की मश्क़ करने लगतीं। उन दिनों नौहे की धुनों पर फ़िल्मी म्यूज़िक का क़ब्ज़ा नहीं हुआ था। नौहों की धुनें देहातों, क़स्बों और छोटे-मोटे शहरों की लोक-धुनों की तरह सादा और साथ-ही-साथ गम्भीर हुआ करती थीं, और जब बाजी, अम्माँ या कोई और खाला या फूफी काले कपड़े पहनकर नौहा पढ़ने खडी़ होतीं :
सोते-सोते सकीना यह कहती उठी शह का सीना नहीं तो सकीना नहीं...तो बयाज़ सँभालनेवाली कलाइयाँ एकदम से बदल जातीं। सुननेवालों को ऐसा मालूम होता जैसे नौहे की आवाज़ खास दमिश्क के बन्दीघर से आ रही है, और देखनेवाली आँखें देख लेतीं कि एक ज़मीनदोज़ क़ैदख़ाने में हुसैन की बहन ज़ैनब हुसैन की चहेती बेटी सकीना को बहलाने की कोशिश कर रही है...
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book